वैसे तो 'राग दरबारी' का प्रकाशन 1968 में हुआ था। यानी आज से लगभग 50 साल पहले। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी यह नहीं लग सकता कि इसमें इतने पुराने दिनों की बात हो रही है। शिवपालगंज को कहीं अलग से खोजने जाने की जरुरत नहीं है। अगर ध्यान से देखिएगा तो हमारे आपके बीच छोटे-बड़े कितने शिवपालगंज, कितने वैद्यजी, कितने रामाधीन भीखमखेड़वी मौज़ूद हैं। यह एक लेखक के लिए गर्व की बात हो सकती है कि उसकी लिखी रचना लिखे जाने के बाद और ज्यादा प्रासंगिक होती जा रही है। इसमें से कुछ बातें अगर उस समय को पाठकों को काल्पनिक लग गयी हों तो आज तो सर्वथा उचित ही लगती हैं। यहाँ एक बात आश्चर्य करने वाली यह है कि यह सब आज़ादी के दो दशकों के भीतर हो गया था। जिस आज़ादी के लिए इतने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी थी उसका विकृत स्वरुप बहुत जल्दी ही बेपर्दा हो गया था।
इस उपन्यास की कहानी किन्हीं मुख्य किरदारों के इर्द-गिर्द नहीं घूमती है। उपन्यास में अनेक पात्र हैं और लगभग सभी किरदारों को समान अहमियत दी गई है। गाँव की राजनीति के दो मुख्य ध्रुव हैं - वैद्यजी और रामाधीन भीखमखेड़वी। वैद्यजी अपरोक्ष रूप से गाँव का कॉलेज, कोआपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं। इस बार प्रधान पद भी वैद्यजी के गुट में आ गया था। रामाधीन के पास अवैध धंधों का एकाधिकार था। वैद्यजी के दो बेटे थे - एक अखाड़े में पहलवानी करते थे और दूसरे कॉलेज में राजनीति और गुण्डागर्दी। रंगनाथ शहर का पढ़ा हुआ एक लड़का है जो कि कुछ दिनों की छुट्टी के लिए शिवपालगंज में अपने मामा वैद्यजी के पास जाता है। ये सभी पात्र शिवपालगंज के रहने वाले हैं। कहानी के स्थानों के वर्णन से यह लखनऊ के पास किसी स्थान की कहानी लगती है, जहाँ अवधी भाषा बोली जाती है।
कहानी में हास्य है लेकिन हास्य केन्द्रित कहानी कह देना अनुचित होगा। कहानी का केन्द्र व्यवस्था में जड़ जमा चुकी अनैतिकता है। अंत में हर एक पात्र का उद्द्येश्य सिर्फ यह रह जाता है कि कोई चीज उसके अनुसार हो रही है कि नहीं। व्यवस्था को सुधारने से किसी का कोई उद्द्येश्य नहीं रह जाता। सरकारी तंत्र के जिन अंगों का यहाँ पर ज़िक्र हुआ है उनका बहुत ही पतित रूप दिखाया गया है चाहे वह पुलिस हो, न्यायालय हो, सरकारी विद्यालय निरीक्षक हों या गाँव के प्रधान ही क्यों न हों। हर एक व्यवस्था को अपने अनुसार ढाल लेना यह कोई इस उपन्यास के पात्रों से सीखे। यह करते समय भी ऊपर से आदर्शवाद का दिखावा बनाये रखा जाता है और भाषणों में आदर्शवाद की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। सामान्य जनता में भी शायद इस बात का भरोसा हो गया है कि जिसके पास शक्ति है वही सब कुछ कर सकता है, अन्यथा व्यवस्था से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से रबर-स्टाम्प लोगों के माध्यम से सत्ता को परदे के पीछे से संचालित किया जाता है।
इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचतान को दिखाया गया है। शहर का पढ़ा हुआ नौजवान जब किताबी आदर्शों को लेकर गाँव पहुँचता है तो उसे हर एक संस्था भ्रष्ट लगती है। वह हर समय यही कोशिश करता रहता है कि कैसे इस व्यवस्था को सुधार जाये। उसने जब देखा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों का पलड़ा कमजोर हो रहा है तो उसने उन लोगों की तरफ से आवाज उठाने की कोशिश भी की और उनको अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानी के विरुद्ध लड़ते रहने के लिए उकसाया भी। इतना सब करने के बाद भी जब उसकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकला तो उसने हार मान ली। और गाँव छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तब कहानी के अन्य पात्र ने उससे कहा कि जाओगे कहाँ। हर जगह तो बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसने इस बात पर सोचा भी कि छोटे बड़े रूप में हर जगह शासन ऐसे ही चलता है। यही इस उपन्यास का मूल तत्त्व कहा जा सकता है कि अनेक बार जब आदर्शवाद और यथार्थवाद टकराते हैं तो बहुधा पहले हार मानने वाला आदर्शवाद ही होता है।
उपन्यास की भाषा में आँचलिकता के तत्व हैं। उत्तर प्रदेश के अवध प्रान्त में बोले जाने वाले बहुत से शब्द इस्तेमाल किये गए हैं। कई जगह सीधे सीधे अवधी भाषा में किये गए वार्तालाप को उद्धृत किया गया है। पूरी पुस्तक के हर एक पैराग्राफ में शासन-व्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया गया है। इस तरह से कहीं भी रूचि कम नहीं होती है। कहानी का अंत थोड़ा अलग है। यह लग सकता है कि अंत अचानक से हो गया है। साथ ही साथ कॉफ़ीहाउस में चलने वाली वैचारिक चर्चाओं पर भी व्यंग कसा गया है जिनका कोई परिणाम निकलकर नहीं आता है लेकिन उसमें भाग लेने वाले अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल को इस कृति के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाज़ा गया था। कटाक्ष का एक उदाहरण देखिये-
".. फिर भी लेक्चर इतने ज्यादा होते थे कि दिलचस्पी के बावज़ूद, लोगों को अपच हो सकता था। लेक्चर का मज़ा तो तब है कि जब सुननेवाले वाले भी यह समझें कि यह बकवास कर रहा है और बोलनेवाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। पर कुछ लेक्चर देनेवाले इतनी गम्भीरता से चलते कि सुननेवाले को कभी-कभी यह लगता था यह आदमी अपने कथन के प्रति सचमुच ही ईमानदार है। ऐसा संदेह होते ही लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था और उसका असर श्रोताओं के हाज़मे के खिलाफ पड़ता है।… ज्यादातर लोग की लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर ऊँघने और शाम को जागने के बीच लेते थे।"
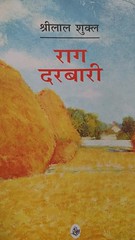
अति उत्तम समीक्षा
ReplyDeleteआपका आभार
सराहनीय ....
ReplyDelete